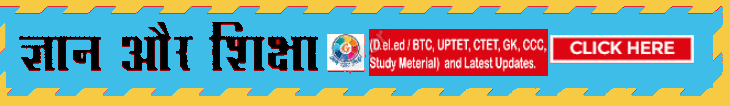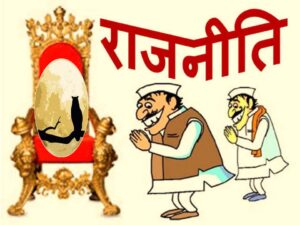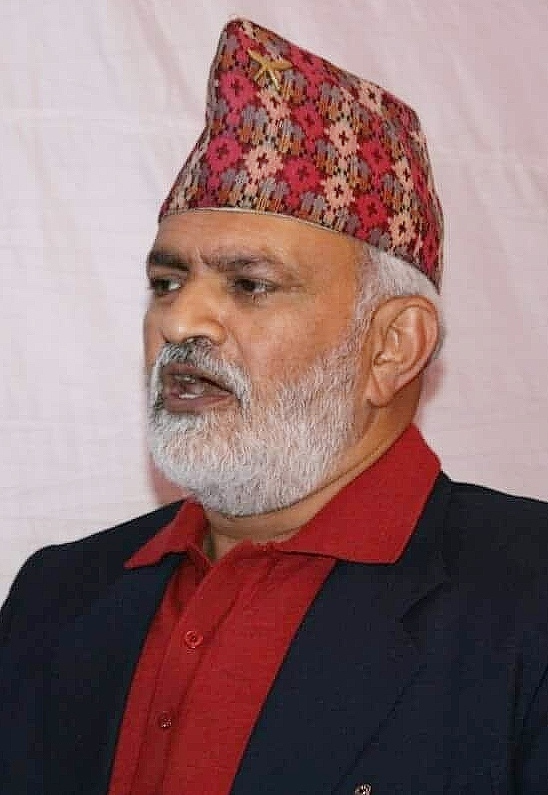
उत्तराखंड में भाजपा का कांग्रेसीकरण होता हुआ देखकर अच्छा लगा। यह देखकर भी अच्छा लगा कि सत्ता का अपना चरित्र होता है और कोई विरला ही उससे अछूता रह पाता है। विगत वर्षों मे कांग्रेस में तो यह सामान्य क्रम होता था कि किसी भी मुख्यमंत्री को कुछ निश्चित समय के बाद हटा ही दिया जाता था (श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में तो प्रसिद्ध था कि वो समय समय पर हिलाकर देखती रहती थीं कि मुख्यमंत्री की जड जमने तो नहीं लग गई है!) और नए मुख्यमंत्री का एक प्रकार से मनोनयन तथाकथित “हाईकमान” के द्वारा किया जाता था। हाईकमान के कुछ अधिक विश्वस्त व्यक्ति को कहीं से भी लाकर विधायक दल के ऊपर थोप दिया जाता था।इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व में यह सब इतनी सरलता से घटित होता रहता था जैसे यह कुछ विशेष न होकर बहुत ही सामान्य घटनाक्रम हो। बडे से बडे कद्दावर नेता , चाहते हुए भी ,कुछ कर नहीं पाते थे। हर परिवर्तन या फेर बदल के बाद श्रीमती गांधी को लगता था कि पार्टी पर उनकी पकड और अधिक मजबूत हो रही है! किसी हद तक यह सही भी था परन्तु पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और स्वयं पार्टी के लिए ये अनावश्यक फेरबदल घातक सिद्ध हुए और पार्टी भीतर ही भीतर खोखली होती चली गई। सामूहिक नेतृत्व का स्थान गुटबाजी ने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्थान प्रतिद्वंदिता ने ले लिया था परन्तु आत्मसम्मोहन के शिकार सत्ताधीश को मुर्गों को लडवाकर अपनी गद्दी सुरक्षित करने का भ्रम आनन्दित करता था।
.. फिर नाटक शुरू होता था लोकतंत्र का। विधायक दल की बैठक होती थी , हाईकमान के ‘पर्यवेक्षक’ आते थे , त्यागपत्र देने वाला मुख्यमंत्री ही, अनिवार्य रूप से,नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करता था , मुख्यमंत्री पद का लगभग समानांतर दावेदार उस प्रस्ताव का समर्थन करता था और तथाकथित ‘सर्वसम्मति’ से सभी विधायक नए नेता का निर्वाचन कर लेते थे। नवनिर्वाचित ( मनोनीत) मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने वाले मुख्यमंत्री की खूबियों का बयान करता था और प्रधानमंत्री/पार्टी अध्यक्ष/हाईकमान का ‘सेवा का अवसर’ प्रदान करने के लिए गुणगान करता था।अगर कहीं कोई विशेष दिक्कत होती थी तो कांग्रेस अध्यक्ष/हाईकमान पर निर्णय छोड दिया जाता था। प्रतिपक्षी दल, विशेष रुप से भाजपा , इस सारी प्रक्रिया की जमकर खिल्ली उड़ाते थे। कांग्रेस पर लोकतंत्र के हनन और तानाशाही प्रवृत्ति का आरोप लगाया जाता था। प्रदेश की जनता का अपमान , जनादेश के उपहास , लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या और न जाने कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता था। मामला कुछ समय यानी पांच सात महीने या वर्ष दो वर्ष के लिए सतही तौर पर सुलझा हुआ समझ लिया जाता था। और कुछ समय पश्चात इस पूरे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती थी। पार्टी में एकजुटता का स्थान गुटबाजी ले लेती थी। वैचारिक प्रतिबद्धता के स्थान पर प्रबंधन का कौशल हावी हो जाता था अर्थात मैनिप्युलेशन और मैनूवरिंग की कला जन सेवा का स्थान ले लेती थी। लोकप्रियता, विधायकों के प्रति जवाबदेही और जनसमर्थन की चिंता का स्थान पार्टी हाईकमान की निकटता या हाईकमान का ‘आशीर्वाद’ ले लेता था।
वर्तमान घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा अपने आपको कांग्रेसी संस्कृति में ढालने को न केवल आतुर और व्यग्र है बल्कि कुछ विशेष प्रकार की हड़बड़ी में है। नित्यानंद स्वामी, भगत दा, जनरल खंडूरी,रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या फिर तीरथ सिंह रावत , क्या इनमें से किसी एक को भी विधायकों की पसंद से चुना हुआ मुख्यमंत्री माना जा सकता है ? कांग्रेस हाईकमान यानी स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तानाशाही और अहंमन्यता का आरोप लगाने वाली भाजपा के आचरण और व्यवहार को क्या लोकतांत्रिक कहा जा सकता है ? त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने का मुख्य कारण अधिकांश विधायकों की अप्रसन्नता या नाराजगी (?) बतलाया जा रहा है। चार वर्षों तक हाईकमान को इसकी सुध नहीं आई और अचानक अंतर्ज्ञान हुआ या आकाशवाणी हो गई कि विधायक प्रादेशिक नेतृत्व से प्रसन्न नहीं हैं और आगामी चुनाव त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में लडना घाटे का सौदा साबित हो सकता है! केंद्र के पास खुफिया एजेंसियां होती हैं और भाजपा के पास तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा समर्पित और जमीन से जुडा संगठन है। संगठन और सरकार में दिन प्रतिदिन के आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान नियमित रुप से होता है। यदि कहीं तालमेल का अभाव था तो उसे दूर करने का प्रयास तो कभी किसी स्तर पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। “चिंतन शिविर” और “मंथन बैठकें” ये किस मर्ज की दवा हैं ? क्या यें सिर्फ कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने वाला दिखावा मात्र थीं? प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री चार वर्षों तक क्या करते रहे? फिर भी , यदि स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी कि नेतृत्व परिवर्तन के बिना काम नहीं चल रहा था , तो क्या इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता फिर भी नहीं समझी गई कि विधायकों का मत, उनकी राय लेना उचित रहेगा। तो फिर क्या विधायकों की राय ली गई ? नहीं । नेतृत्व परिवर्तन की जल्दबाजी में यह विचार करना भी आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ कि एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाने से दो दो उपचुनाव -एक विधानसभा के लिए और दूसरा लोकसभा के लिए लडने पड़ेंगे ! यह विचार भी नहीं किया गया कि इससे पार्टी में अनावश्यक गुटबाजी भी बढ सकती है।जिस रोग से कांग्रेस हाईकमान ग्रस्त
था , उसी रोग ने भाजपा को भी जकड और पकड लिया है।
जो स्थिति आज उत्पन्न हो गई है , यह केन्द्रीय नेतृत्व की विफलता है, इसके लिए केवल और केवल नेतृत्व की विफलता उत्तरदाई है। क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि वर्तमान विधायकों में कोई एक भी प्रदेश का नेतृत्व करने की योग्यता नहीं रखता ?
आज भाजपा अकारण ही एक मनोवैज्ञानिक युद्ध हार गई है और कांग्रेस को प्रदेश में एक मनोवैज्ञानिक बढत हासिल हो गई है। 2022का चुनाव सिर पर है और आप मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने में उलझे हुए हैं। विधायकों की पसंद, इच्छा और वरीयता को दरकिनार कर आपको भी कठपुतली मुख्यमंत्री बनाने का रोग लग चुका है। इन मूर्खतापूर्ण प्रयोगों का दुष्परिणाम कांग्रेस झेल रही है लेकिन उनसे सबक लेने के बजाए आप उन्हें दोहरा रहे हैं और वो भी उसी हास्यास्पद तरीके से। अतिआत्मविश्वास और अहंकार में बहुत पतली ,बारीक रेखा होती है। उसका उल्लंघन या अतिक्रमण कब हो गया , यह पता मुश्किल से और बहुत देर बाद चलता है और जब पता चलता है तब तक बडा नुकसान हो चुका होता है।
मेरे विचार से तीरथ सिंह रावत तो कभी भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपने आपको दावेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व ने उन्हें अकारण ही उपहास का पात्र बना दिया है। छ:महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता की संवैधानिक अनिवार्यता की अनदेखी करना क्या सिद्ध करता है?उनके बहिर्गमन को किसी भी दृष्टि से सम्मानजनक तो नहीं कहा जा सकता है। उत्तराखंड में इस अतिआत्मविश्वास ने भाजपा को हास्यास्पद स्थिति में लाकर खडा कर दिया है। सामान्य कार्यकर्ता हतप्रभ है और किंकर्तव्यविमूढ़ सा केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व की तरफ देख रहा है।वह देख रहा है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और वह असहाय है।एक अलग “चाल , चरित्र और चेहरे” वाला दल राजनीति के मैदान में खेल के उन्ही नियमों को आत्मसात कर रहा है जिनका पुरजोर विरोध वह राजनीति के रंग मंच पर बहुत ऊंचे स्वर में करता था।
समाजविज्ञानियों या राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों को अध्ययन करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही और अधिनायकवादी प्रवृतियां क्यों पनप रहीं हैं ? दलों का नेतृत्व/हाईकमान अपनी ही पसंद( क्योंकि टिकट तो वही देते हैं) और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है ? एक लोकप्रिय पुराने शेर को कुछ परिवर्तन के साथ ऐसे कहा जा सकता है…….
हर शाख पे उल्लू बैठा है
अंजामे लोकतंत्र क्या होगा?